यह घटना सूचना का अधिकार कानून कि ताकत की सक्सेस स्टोरी है | इस ताकत को हमने आजमाया है |इसकी सिर्फ जानका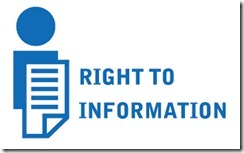 री होना ही काफी नहीं है बल्कि इसको आजमा कर देखना चाहिए | अगर देश का हर जागरूक इंसान ऐसे अपनी मुश्किलों में इस कानून का इस्तेमाल करेगा तो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए किसी लोक पाल बिल की जरूरत नहीं |
री होना ही काफी नहीं है बल्कि इसको आजमा कर देखना चाहिए | अगर देश का हर जागरूक इंसान ऐसे अपनी मुश्किलों में इस कानून का इस्तेमाल करेगा तो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए किसी लोक पाल बिल की जरूरत नहीं |
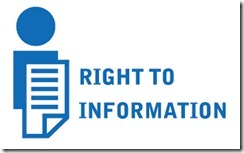 री होना ही काफी नहीं है बल्कि इसको आजमा कर देखना चाहिए | अगर देश का हर जागरूक इंसान ऐसे अपनी मुश्किलों में इस कानून का इस्तेमाल करेगा तो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए किसी लोक पाल बिल की जरूरत नहीं |
री होना ही काफी नहीं है बल्कि इसको आजमा कर देखना चाहिए | अगर देश का हर जागरूक इंसान ऐसे अपनी मुश्किलों में इस कानून का इस्तेमाल करेगा तो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए किसी लोक पाल बिल की जरूरत नहीं |
बात पिछले दो साल की है | दिन व तारीख तो याद नहीं, हाँ इतना पता है कि उस दिन सूर्य ग्रहण पड़ा था | ग्रहण खग्रास नहीं खण्ड ग्रास था | ऐसा नहीं कि ग्रहण होने की वजह जयपुर थम गया हो लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से लोग रहे होंगे जो उस वक्त घर से नहीं निकले होंगे | दो तीन तो हमारे ऑफिस में ही थे जिन्होंने खुले में जाने से परहेज किया | बावजूद इसके मैं और मेरा दोस्त जो कि मेरा सहकर्मी भी है ने इन दो घंटों का इस्तेमाल एक महत्वपूर्ण काम को करने में किया | काम दरअसल यह था कि मेरे दोस्त भँवर ने बताया कि उन्होंने LIC (जीवन बीमा) की एक पॉलिसी विड्रो करवाई थी, तीन - चार महीने पहले | लेकिन भुगतान का चैक जो कि एक सप्ताह में उनके पास पहुंचना चाहिए था वह अभी तक उनके पास नहीं पहुंचा था | इसके लिए भँवर जी उनके ऑफिस में कई चक्कर लगा चुके थे | कई बार फोन भी किया | कभी काम से सम्बन्धित जिम्मेदार व्यक्ति सीट पर नहीं होता तो कभी मिल जाता तो प्रकिया में है कह कर टरका देता | ग्रहण वाले दिन हमने योजना बनाई कि क्यों न हम (RTI) सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अर्जी लगाकर पता तो करे कि मामला कहाँ अटका हुआ है ? भंवर जी ने कहा कि यह ठीक बात है “हम दूसरों को तो सूचना का अधिकार के लिए जाग्रत करते हैं, आज खुद के लिए भी कर के देखें | तुरंत हमने एक अर्जी सूचना अधिकारी , जीवन बीमा कार्यालय जयपुर के नाम लिखी | याद रखें सूचना अधिकारी नाम का प्राणी हर कार्यालय में होता है | और कार्यालय की किसी दीवार पर उसका नाम भी चस्पा होना चाहिए | तो हमने लिखा कि हमें सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ तहत निम्न लिखित जानकारियां चाहिए -
- मेरे काम में हो रहे विलम्ब का यथोचित कारण बताएँ |
- मेरे काम की अब तक की प्रगति की स्थिति बताएँ | तथा
- मेरे काम के लिए कौन-कौन व्यक्ति जिम्मेदार हैं | उनके नाम बताएँ ताकि प्रमाद पाए जाने पर जरूरी कानूनी कार्यवाही उनके खिलाफ की जा सके |
अर्जी लिखने तक सूर्य ग्रहण कि गिरफ्त में आ चूका था | और हम तय कर चुके थे कि आज हम और सूर्य एक साथ ग्रहण से निकलेंगे | सूर्य चन्द्रमा की छाया से और हम भ्रष्टाचार की गिरफ्त से | हम सीधे LIC ऑफिस पहुंचे | सेकंड फ्लोर पर बड़ा सा हॉल, हॉल में कुर्सियां ही कुर्सियां … कुर्सियों के आगे मेजें ही मेजें … मेजों पर फाइलों के ढेर … कुछ कुर्सियों पर बाबू लोग आसीन, कुछ पर टंगे कोट… इसके अलावा भी बहुत साजो सामान |
जैसा हम सोच रहे थे वैसा यहाँ कुछ भी नहीं था | यहाँ किसी भी कोने पर सूचना अधिकारी का नाम नहीं लिखा था | क्या करें, किससे पूछें ? इसी उहापोह में एक टेबल पर फाइलों से झांकते हुए हमने एक बड़े ऑफिस कर्मी से पूछ लिया “ यहाँ का सूचना अधिकारी कौन है ?” इस एक वाक्य ने जैसे वहाँ रुके हुए पानी में पत्थर मार दिया हो | अभी तक जो सभी जो एक दूसरे से असम्प्रक्त से अपनी गतिविधियों में मस्त थे | कही बातचीत भी तो ‘वोटिंग फॉर गोडो’ के पात्रों की तरह उकताहट मिटाने की विवशता युक्त प्रयास –सी | इस एक वाक्य ने सब को जोड़ कर रख दिया | सबकी नज़रें हम पर केंद्रित हो गईं | ऐसे सवाल से सामना करने की उम्मीद किसी को नहीं थी | हमने फिर अपना सवाल दोहराया | वह चुप , चुप्पी कुछ सघन हो गयी थी क्योंकि उसकी चुप्पी में अब सभी चुप्पियाँ शामिल हो गयीं थीं और मानो उन सब चुप्पियों ने एक बड़े सन्नाटे का निर्माण कर दिया हो | वह सन्नाटा जैसे हमसे ही सवाल कर रहा था - वाह ! भला यह भी कोई बात है ? ऐसा भी कहीं होता है ? अरे भाई कानून है तो क्या लेकिन काम तो काम के तरीके से ही होता है ! सन्नाटे कागुब्बारा जल्दी ही फूट गया | उसे हमने ही फोड़ा यह कह कर “ हमें सूचना अधिकारी का नाम बताइए हमें अर्जी लगानी है और आपने यहाँ उसका नाम भी नहीं लिख रखा जो कि यहाँ होना चाहिए |” इतने में ही भंवर जी ने अर्जी टेबल पर दे मारी | मगर मजाल है किसी ने उसे छुआ, अर्जी नहीं जैसे वर्जित फल हो ! इतने में ही पीछे से आवाज़ आयी आपको मैनेजर साब ने बुलाया है | हम मैनेजर के केबिन में चले गए | हमारा प्रयोजन पहले ही प्रेषित था, भूमिका पहले ही बन गई थी | इसलिए बिना भूमिका के हमने अर्जी सरकाई | साहब ने पढ़ी , साहब की घंटी घनघनाई , तुरंत एक महिला कर्मचरी आई … साहब बोले , “ इन सर का काम क्यों नहीं हुआ ?”
कर्मचारी बोलीं , “ सर …सर.. इनका…वो ….जो …जो छुट्टी पर … मैनेजर बोला , “ वो छुट्टी पर है तो क्या काम नहीं होगा … जाओ फोरन इनका चेक बना कर लाओ| "
अगले १० मिनट में चैक भँवर जी के हाथ में था |
मैनेजर बोले, “ कोई और काम हो तो जरूर बताएँ |”
हम बोले, “ अभी तो काम यही है कि आप इस अर्जी को विधवत लगाओ |”
मैनेजर - अब तो रहने दो आपका काम तो हो गया |
हम - पता तो चले कि चूक कहाँ है ?
सारांश यह है कि मैनेजर ने कहा कि आप जिसकी गलती है माफ़ कर दीजिए .. नौकरी … बाल बच्चों का सवाल …
हम चलने लगे तो मैनेजर ने कहा कि आप यह अर्जी मुझे देते जाओ ताकि मैं अपने स्टाफ को दिखा सकूँ कि अब पुराने वाला तरीका नहीं चलेगा |
जब हम वहाँ से निकले तो ग्रहण हट चूका था सूर्य का भी और भ्रष्टाचार का भी | लेकिन ग्रहण तो आते रहते हैं | लेकिन जज्बा सूरज वाला होना चाहिए जो हर बड़े ग्रहण के बाद निकल के आता है नयी रौशनी के साथ |
(मेरे दूसरे ब्लॉग बतकही से)







